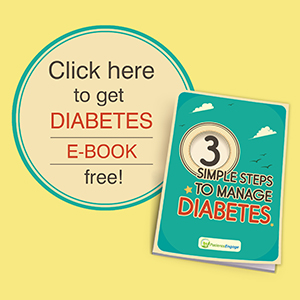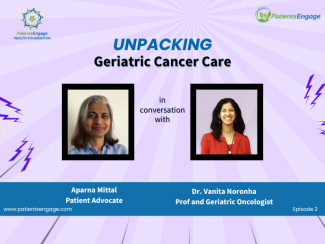
प्रमुख मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और शोधकर्ता डॉ. वनिता नोरोन्हा ने पेशेंट्सएंगेज पॉडकास्ट पर बुजुर्गों में कैंसर देखभाल के लिए आवश्यक विशेष वृद्धावस्था संबंधी मूल्यांकन के बारे में चर्चा की, और बताया कि ऐसे मूल्यांकन से उपचार को व्यक्तिगत बनाने में कैसे मदद मिल सकती है। जानकारी के लिए पढ़ें पॉडकास्ट पर आधारित यह लेख:
जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी या जेरीऐट्रिक कैंसर केयर (बुजुर्गों के कैंसर उपचार और देखभाल के क्षेत्र) क्या हैं?
जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी या जेरीऐट्रिक कैंसर केयर (बुजुर्गों के कैंसर उपचार और देखभाल के क्षेत्र) क्या हैं?
जेरीऐट्रिक का अर्थ है वृद्ध लोगों से संबंधित (खासकर उनके स्वास्थ्य से संबंधित), और जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी का अर्थ है बुजुर्गों में होने वाले कैंसर के उपचार से संबंधित क्षेत्र। उम्र बढ़ने के साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर और अंग प्रणालियों में भी बदलाव होते हैं और लोगों में गिरने, कमज़ोरी, बीमारियों/ प्रतिरक्षा में कमी जैसी स्थितियों की संभावना भी बढ़ती है। उम्र बढ़ने के कुछ स्पष्ट लक्षण से तो हम परिचित हैं, जैसे कि झुर्रियां, पर शरीर के अंदर मांसपेशियाँ, यकृत, गुर्दे, हृदय और अन्य आंतरिक अंग भी उम्र के साथ बदलते हैं, भले ही ये झुर्रियों बदलाव बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इसलिए, वृद्ध लोगों में सभी चिकित्सा उपचार इन बदलावों को ध्यान में रख करना होता है, और इसलिए वृद्धावस्था में होने वाले कैंसर के प्रबंधन की आवश्यकताएं भी अलग होती है। बुजुर्गों में कैंसर के अलावा, अन्य मौजूदा कमज़ोरियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी होती है। इससे कैंसर की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलती है और व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में भी मदद मिलती है।
Read summary in English: https://www.patientsengage.com/news-and-views/unpacking-geriatric-cance…
वृद्धावस्था कैंसर असेसमेंट टेस्ट कब किया जाता है और इसमें किन कारकों पर विचार किया जाता है?
किस उम्र में व्यक्ति को “वृद्ध” माना जाता है, इस की परिभाषा अलग-अलग स्थानों और संस्थाओं में अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित “वृद्ध” माना जाने के लिए मानक आयु 65 वर्ष है (अमेरिका और यूरोप में यह 65 वर्ष । इस आयु और इस से अधिक आयु वाले लोगों में कैंसर के उपचार को जेरिएट्रिक ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत माना जाता है। “वृद्ध” आयु सीमा देश के अनुसार भिन्न होती है, और यह सीमा उस देश की सेवानिवृत्ति की आयु और जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, और सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है और व्यक्ति का सामाजिक दायरा भी बदल जाता है। पर ध्यान रहे, यह कालानुक्रमिक आयु है (व्यक्ति कितने साल से जिंदा हैं) पर स्वास्थ्य के संदर्भ में शारीरिक आयु अधिक उपयुक्त है। कैंसर वाले व्यक्ति का आकलन शारीरिक आयु से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है पर वे दुर्बल हैं, उन्हें कोई क्रानिक बीमारी है, वे लकवाग्रस्त हैं, वे किसी दुर्घटना में थे, आदि, तो उनकी शारीरिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से बहुत अधिक हो सकती है। कैंसर के आकलन के लिए शारीरिक आयु का उपयोग किया जाता है – यह देखा जाता है कि व्यक्ति की आयु के स्वस्थ लोगों की तुलना में व्यक्ति कार्य कैसे कर रहे हैं। यह आकलन जेरिएट्रिक असेसमेंट टेस्ट या जीएटी के माध्यम से किया जाता है।
जेरिएट्रिक असेसमेंट टेस्ट (जीएटी) क्या है?
जेरिएट्रिक असेसमेंट टेस्ट (यानि कि जीएटी) एक ऐसा मूल्यांकन है जो कैंसर के अलावा कई अन्य पहलुओं पर आधारित है और व्यक्ति का मूल्यांकन उनकी शारीरिक आयु बनाम कालानुक्रमिक आयु के आधार पर करता है। जीएटी उन गैर-कैंसर पहलुओं का मूल्यांकन करता है जो व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से जीने और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इसमें सह-रुग्णताएँ शामिल हैं – जैसे कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियाँ, और संबंधित दवाओं का सेवन या पॉलीफार्मेसी (जिसमें 5 या अधिक दवाओं का सेवन शामिल है) ताकि व्यक्ति के द्वारा ली जाने वाली दवाओं के बीच परस्पर क्रियाओं को समझा जा सके।
यह मूल्यांकन यह समझने के लिए भी किया जाता है कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र रूप से कितनी अच्छी तरह अपने कार्य कर सकते हैं, और दैनिक गतिविधियाँ कैसे कर सकते हैं। इसमें शामिल कुछ पहलुओं के उदाहरण - मांसपेशियों की ताकत, गिरने का जोखिम, अस्पताल में भर्ती होने के लिए आवश्यक सामाजिक सहायता प्रणाली, दवाएँ खरीदना और उनका भुगतान करना, खाना बनाना, देखभाल करना, आदि। यह सब जीएटी का हिस्सा हैं और हम प्रश्नों के एक समूह के आधार पर व्यक्ति की सभी कमजोरियों को समझते हैं। हम विभिन्न मान्य प्रश्नावली का उपयोग करके इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर देखा जा सकता है कि क्या व्यक्ति को “फ्रेल” (दुर्बल, कमजोर) के रूप में वर्गीकृत करना उचित होगा। इन उत्तरों के आधार पर, हम व्यक्ति के लिए उचित कदम के सुझाव दे पाते हैं – जैसे कि घरेलू व्यायाम कार्यक्रम, जरूरत के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक से सहायता लेना, यहाँ तक कि बाथरूम में हैंडल लगाने और वॉकिंग गेट इस्तेमाल करने का सुझाव देना।
हम व्यक्ति की कमज़ोरियों को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यदि आकलन में पाया जाए कि व्यक्ति की क्षमता दो या अधिक क्षेत्रों में कम है, तो व्यक्ति को “फ्रेल” श्रेणी में रखा जाता है। इस वर्गीकरण से यह तय करने में मदद मिलती है कि व्यक्ति को किस तरह के इलाज और सहारे की ज़रूरत है।
जीएटी के लिए रेफरल प्रणाली क्या है? जीएटी कब करवाना चाहिए?
दुर्भाग्यवश, भारत में वृद्धों में कैंसर की देखभाल के लिए विशिष्ट कदमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जीएटी करवाने से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है और कैंसर के इलाज के लिए की गई कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं। भारत में जीएटी पर अधिक जानकारी और जागरूकता नहीं है और इसके लिए कोई सुस्थापित औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम भी मौजूद नहीं है। केवल कुछ ही चिकित्सक जीएटी कर पाते हैं और वर्तमान में बहुत की कम केस में व्यक्ति को इस के लिए रेफर किया जाता। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में इसमें बदलाव आ रहा है।
टाटा मेमोरियल अस्पताल में एक बहु-विषयक जराचिकित्सा ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है और जिन बुजुर्ग व्यक्तियों के कैंसर उपचार के लिए निर्देशित चिकित्सा की योजना बनाई जाती है, और उन्हें चिकित्सा से पहले यहाँ रेफर किया जाता है, ताकि किसी भी कमी या कमज़ोरी का पता लगाया जा सकता है और आवश्यकतानुसार कदम लेकर उसे दूर किया जा सके। फॉलो-अप कार्रवाई के दौरान, खासकर जब उपचार में कोई बदलाव होता है, तो जीएटी दुबारा किया जाता है ताकि पता चले कि विभिन्न क्षेत्रों में कमजोरी की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है।
क्या आप कुछ उदाहरण देकर समझा सकती हैं कि यह आकलन व्यक्ति की सामान्य नैदानिक जाँच से ज़्यादा सटीक क्यों होता है? क्या यह कुछ कैंसर के प्रकार वाले लोगों के लिए अन्य कैंसर के प्रकार की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त है?
जीएटी कैंसर-विशिष्ट नहीं, बल्कि उम्र-विशिष्ट है और कैंसर की किसी भी अवस्था के लिए यह करवाने की सलाह देना उचित है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी कैंसर वाले व्यक्ति को जीएटी करवाने की सलाह दी जानी चाहिए। प्रोस्टेट या जननांग-मूत्राशयी अंगों के कैंसर जैसे कुछ कैंसर मुख्य रूप से वृद्ध लोगों की बीमारी हैं, जिनके लिए जीएटी किया जाना चाहिए।
अकसर क्लीनिक बहुत व्यस्त होते हैं और जीएटी में समय लगता है। ऐसे में भी सही आकलन के लिए जीएटी किया जाना चाहिए - तुरंत निर्णय लेने के लिए सिर्फ व्यक्ति को देख कर उनका आकलन नहीं किया जाना चाहिए। कई डॉक्टर सिर्फ व्यक्ति को देख कर यह निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति कैंसर का इलाज सहन कर पाएंगे या नहीं। परंतु ऐसे अंदाजन आकलन 50% बार जीएटी द्वारा किए गए आकलन की तुलना में गलत होते हैं। व्यक्ति की कुछ कमज़ोरियाँ आसानी से नजर आ जाती हैं, और इन से आकलन में मदद मिलती है, उदाहरण के लिए, अगर वे गिर गए थे और उनकी गतिशीलता में कमी है / वे कार्यात्मक रूप से कमज़ोर है। पर कुछ पहलू सिर्फ व्यक्ति को देखने से पता नहीं चलते हैं, खासकर संज्ञानात्मक हानि, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, या सामाजिक या वित्तीय सहायता का अभाव।
व्यक्तियों की भावनाओं के बारे में सरल और स्पष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाती है। कई बार ऐसे प्रश्नों का उत्तर अक्सर देखभाल करने वाले भी द्वारा आसानी से दे पाते हैं। पर सिर्फ व्यक्ति को देखने से, कुछ काम करवाने से, सरल प्रश्न पूछने से, या उनके पोषण का मूल्यांकन करके भी कुछ ऊपर दिए गए पहलुओं का सही आकलन नहीं हो सकता। खासकर ग्रामीण लोगों के मामलों में, जो खेतों में काम करते हैं, हो सकता है कि उनके शरीर का वजन कम हो और वे कुपोषित दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में कुपोषित नहीं हैं। जब कैंसर वाले व्यक्ति खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो मूल्यांकन रिश्तेदार द्वारा या वीडियो के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति मूल्यांकन के लिए मौजूद हों तो अधिक विस्तार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और व्यक्ति के वजन और अन्य बातों पर जानकारी मिल सकती है।
एक अन्य पहलू है गुर्दों की कार्यक्षमता जो किड्नी फंक्शन टेस्ट से देखी जाती है – रक्त परीक्षण से क्रिएटिनिन को मापा जा सकता है जिस से गुर्दों के स्वास्थ्य पर जानकारी मिले, पर उम्र के साथ क्रिएटिनिन कम हो सकता है और उस का यह मतलब नहीं कि गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं – इस के लिए कुछ अन्य स्कैन भी जरूरी हैं। चूँकि उम्र के साथ मांसपेशियाँ कम होती हैं, तो क्रिएटिनिन कम होता है, इसलिए उत्सर्जित क्रिएटिनिन भी कम होगा।
व्यक्ति या उनका परिवार यह कैसे पता लगा सकता है कि उन्हें जीएटी की आवश्यकता है या नहीं? वे भारत में इस मूल्यांकन को करने वाले स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को कैसे ढूंढ सकते हैं?
ऐसे कुछ केंद्र हैं जो जीएटी करते हैं - टाटा मेमोरियल में एक जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है जो मुंबई और वाराणसी में यह मूल्यांकन करता है। चेन्नई में भी एक अस्पताल है। आदर्श रूप से सभी कैंसर केंद्रों में जीएटी होना चाहिए क्योंकि यदि जीएटी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इसे सीखना मुश्किल नहीं है। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही जीएटी करें; प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर या नर्स भी यह टेस्ट कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल में जराचिकित्सा ऑन्कोलॉजी फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है।
जीएटी कैसे किया जाता है? क्या इसे व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं?
इसे स्वयं नहीं किया जा सकता। एक ऐप विकसित किया जा रहा है जिसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसका एक बड़ा भाग व्यक्ति खुद भर सकते हैं और एक भाग ऐसा है जिसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा भरा जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता का भाग भरने के बाद उसको समझना भी महत्वपूर्ण है, और यह विश्लेषण एक जीएटी प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए।
क्या जीएटी का संचालन व्यक्ति और उनके परिवार दोनों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए? आप इस प्रक्रिया में व्यक्ति की स्वायत्तता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
शुरु में, व्यक्ति और देखभालकर्ता को प्रश्नावली दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि व्यक्ति स्वयं इसे भरने का प्रयास करें, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति को देखभालकर्ता से अलग-थलग न किया जाए, क्योंकि अंततः देखभालकर्ता ही व्यक्ति का सहायक तंत्र होते हैं। कई बार, देखभालकर्ता का अनुरोध होता है कि सीधे व्यक्ति से बात न की जाए, और ऐसे में यह प्रक्रिया और कठिन हो जाती है।
चिकित्सा देखभाल में एक अवधारणा है कि निर्णय आपस में चर्चा करके, साथ में मिल कर लेने चाहिएं। वृद्ध और कमज़ोर लोगों को भी अपने उपचार के प्रकार पर निर्णय लेने का अधिकार है ताकि वे अपनी आयु बढ़ा सकें और अपनी जीवन की गुणवत्ता भी बनाए रखें। तथ्यों को साझा करते समय कोशिश रहती है कि प्रस्तुति संवेदनशील, संतुलित और सौम्य तरीके से की जाए। यह विशेष रूप से उन्नत और उपशामक देखभाल की स्थिति के लिए जरूरी है क्योंकि ऐसी स्थिति में उद्देश्य यह है कि व्यक्ति आराम से रहें और उन्हें दर्द कम हो, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए, भले ही उपचार से उनका कैंसर कम नहीं हो रहा है। यदि व्यक्ति कम उम्र के हैं और उनकी प्राथमिकताएँ, ज़िम्मेदारियाँ और कुछ आकांक्षाएँ अलग हैं, तो चर्चा भी अलग तरह से होती है।
मूल्यांकन के बाद क्या होता है? इस के आधार पर उपचार की दिशा कैसे बदल सकती है? इस बदलाव पर आप उपचार करने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कैसे काम करती हैं?
जीएटी के स्कोर की मदद से व्यक्ति की स्थिति के बारे में निर्णय लिया जाता है कि क्या व्यक्ति संज्ञानात्मक रूप से क्षीण हैं और क्या उन्हें सह-रुग्णताएं हैं और वे कार्यात्मक रूप से क्षीण हैं और इस सब के आधार पर देखा जाता है कि क्या व्यक्ति को “फ्रेल” में वर्गीकृत किया जाए। व्यक्ति और देखभाल करने वाले को कमजोरियों से जूझने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पर सलाह दी जाती है। संभव सुझाव के क्षेत्र हैं - फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, संज्ञानात्मक क्षीणता के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रॉक्सी, वर्तमान दवाओं की समीक्षा आदि।
इस बात का आकलन किया जाता है कि इस की क्या संभावना है कि व्यक्ति में गंभीर विषाक्तता विकसित होगी जिस के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले हो सकती है। व्यक्ति और उनकी देखभाल करने वालों के साथ इस पर चर्चा की जाती है। यह जानकारी उपचार करने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दी जाती है ताकि ऑन्कोलॉजिस्ट इस को ध्यान में रखते हुए उपचार की खुराक में आवश्यक बदलाव कर पाएं। यह देखा गया है कि जीएटी से प्राप्त जानकारी के आधार पर 35-40% केस में उपचार की योजनाओं को बदला जाता है और ज्यादातर मामलों में जीएटी के आधार पर बदलाव में कीमोथेरेपी की खुराक को कम किया जाता है। अधिकांश रिसर्च ट्रायल में पाया गया है कि जीएटी से प्राप्त लाभ कीमोथेरेपी से जुड़े रहे हैं। विकिरण चिकित्सा (रेडीऐशन थेरपी), सर्जरी जैसे अन्य क्षेत्रों में जीएटी से उपलब्ध जानकारी के प्रभाव पर ज्यादा डेटा नहीं है। सर्जरी के लिए व्यक्ति की फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए प्रीहैबिलिटेशन पर भी ध्यान दिया जाता है।
जीएटी के आधार पर प्रीहैब/रिहैब और अन्य सहायक देखभाल में क्या बदलाव हो सकते हैं? क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं?
जीएटी मूल्यांकन के परिणाम प्रीहैब या रिहैब देखभाल को निर्धारित करते हैं। हम संज्ञानात्मक या शारीरिक व्यायाम, धूम्रपान निषेध जैसे निर्देशित हस्तक्षेप शुरू करने का प्रयास करते हैं।
बुजुर्गों में कैंसर वाले लोगों में उपशामक देखभाल की क्या भूमिका है और आप इसे कब शुरू करती हैं?
कैंसर वाले बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जोड़ी गई ऑन्कोलॉजी उपचार टीम एक बहु-विषयक जराचिकित्सा टीम होती है और इसमें अभिन्न अंग के रूप में एक उपशामक देखभाल (पैलीएटिव केयर) चिकित्सक शामिल किया जाता है। यह उपशामक देखभाल चिकित्सक दर्द प्रबंधन और सामाजिक एवं कार्यात्मक सहायता जैसे कई अन्य क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक बातचीत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए आवश्यक हैं।
क्या भारत में कोई ऐसे सांस्कृतिक या सामाजिक-आर्थिक कारक हैं जो कैंसर वाले बुजुर्गों की देखभाल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं?
जीएटी के अंतर्गत किए गए सभी आकलन पश्चिमी देशों में परिभाषित हुए हैं, इन परीक्षणों में से किसी की भी उत्पत्ति या आविष्कार भारत में नहीं हुआ है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि इन से संबंधित क्या कोई सांस्कृतिक बारीकियाँ हो सकती हैं, या क्या इन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सांस्कृतिक रूप से भारत के लिए अनुपयुक्त हैं।
एक पहलू है दैनिक जीवन की गतिविधियां, जिन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है – वे बुनियादी दैनिक गतिविधियां जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वयं की देखभाल स्वतंत्र तरह से करने के लिए चाहिएं (जैसे कि खुद खाना खा पाना, कपड़े पहनना, नहाना, आदि), और फिर वे सहायक गतिविधियां जो कुछ अधिक मुश्किल हैं और व्यक्ति की सामाजिक व मानसिक क्षमता और व्यवहारिक स्वतंत्रता से संबंधित - इन्हें कई स्थितियों में अन्य लोग भी कर सकते हैं (जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, पैसे का प्रबंधन, खरीदारी करना)। इस दूसरी श्रेणी की गतिविधियों को आईएडीएल (इन्सट्रूमेंटल ऐक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग) कहते हैं और इसके आकलन के लिए 8 प्रश्न पूछे जाते हैं – संतोषजनक माने जाने के लिए महिला को सभी 8 और पुरुषों को 5 करने होते हैं। आकलन में देखा जाता है कि अब की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना अंतर है।
भारत में, अगर घर में बहू होती है, तो सास कई सहायक गतिविधियाँ करना लगभग बंद कर देती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में पहले और वर्तमान की स्थिति में मुकाबला करना मुश्किल होता है।
एक और उदाहरण है संज्ञानात्मक कार्यों के आकलन के लिए वह प्रश्न जिसमें घड़ी (और उसकी घंटे और मिनट की सुईओं) का चित्र बनाना – यह देखा गया है कि भारत में बहुत कम लोग इस प्रश्न को समझ पाते हैं।
सामाजिक सहायता संबंधी प्रश्नों में कुछ अनुकूलन भी भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक पाया गया है - हैं, जैसे यह प्रश्न कि "क्या आपके पास अपनी समस्याएँ साझा करने के लिए कोई है?" यह प्रश्न पश्चिमी देशों में मूल्यवान लगता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होता।
इसलिए भारत के लिए उपयुक्त एक विशिष्ट प्रश्नावली की आवश्यकता है और इसे विकसित किया जा रहा है।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दुर्बलता या संज्ञानात्मक कमी जैसी सह-रुग्णताएँ बुजुर्गों में कैंसर उपचार योजना और परिणामों को कैसे प्रभावित करती हैं?
बुजुर्ग लोगों में सह-रुग्णता एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर यदि सह-रुग्णता नियंत्रित न हो। यदि सह-रुग्णता नियंत्रित हो तब भी बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि व्यक्ति इन रोगों के लिए कई दवाएं ले रहे होंगे, और इन सब का आपस में और कैंसर के उपचार के साथ परस्पर असर हो सकता है, और दवाओं के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और इन सब से उपचार में अधिक जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वृद्ध लोगों में इस से उत्पन्न जोखिम इतना अधिक है कि यह कैंसर जैसे ही जानलेवा हो सकता है।
उदाहरण के लिए, हार्ट फैल्यर एक उन्नत और जीवन को सीमित करने वाली सह-रुग्णता है, जबकि निम्न श्रेणी का प्रोस्टेट कैंसर इतना खतरनाक नहीं है। यदि व्यक्ति को दोनों समस्याएं हैं तो हो सकता है कि उन्हें कैंसर का इलाज करने की आवश्यकता नहीं हो क्योंकि कैंसर उनके हृदय संबंधी मौजूदा सह-रुग्णता जितना जीवन को सीमित करने वाला नहीं है।
इसलिए, नॉन-ऑन्कोलॉजिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे उपकरण/कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है, जिस में सभी आँकड़े दर्ज किए जाते हैं और जिससे प्राप्त परिणाम यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति की मौजूदा स्थिति (कैंसर को छोड़ कर) जीवन प्रत्याशा को कैसे प्रभावित करेगी, और यह निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत में बुजुर्गों के कैंसर उपचार संबंधी प्रणालिओं से संबंधी कमियाँ और चुनौतियाँ (चिकित्सा संबंधी, सामाजिक या विस्तृत प्रणालीगत)
क्या आपको लगता है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली वृद्धावस्था कैंसर वालों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है?
जीएटी अंग्रेजी में उपलब्ध है और हिंदी, मराठी और बंगाली में अनुवादित है क्योंकि ये टाटा मेमोरियल अस्पताल में आने वाले लोगों की सामान्य भाषाएँ हैं, लेकिन सभी स्थानीय भाषाओं में एक संपूर्ण मान्य प्रणाली अभी तक मौजूद नहीं है।
आपके विचार से भारत में वृद्धावस्था कैंसर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किन सुधारों—संसाधनों, प्रशिक्षण, नीति या बुनियादी ढाँचे में—की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?
भारत में इस विषय पर कोई स्थानीय वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। दो संस्थाएं हैं - जिनेवा स्थित एसआईओजी - इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ़ जेरिएट्रिक ऑन्कोलॉजी - नामक एक यूरोपीय जेरिएट्रिक ऑन्कोलॉजिकल संस्था, और सीएआरजी - कैंसर एंड एजिंग रिसर्च ग्रुप - नामक एक अमेरिकी संस्था है, और इन दोनों की वेबसाईट में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है।
टाटा मेमोरियल अस्पताल का एक ऑनलाइन जेरिएट्रिक कैंसर सहायता समूह है, जिसकी महीने में एक बार मीटिंग होती है जिस में आहार और योग जैसे विषयों पर चर्चा होती है और उसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र भी होता है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति या कैंसर वाले वृद्ध व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। सलाह देने के लिए, और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन वर्तमान में तो नहीं उपलब्ध है, पर वे यह उपलब्ध करवाने पर विचार करने को तैयार हैं।
जराचिकित्सक (जेरीऐट्रिशियन) और जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी की वकालत करना और उसे मुख्यधारा में लान
भारत में फिलहाल जराचिकित्सक सीमित संख्या में हैं और पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन अब भारत भर में बड़ी संख्या में जराचिकित्सा कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जिसके कारण जराचिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है। जेरीऐट्रिक्स और ऑन्कोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त लगभग कोई भी स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी उपलब्ध नहीं हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के इस अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मूल समस्या है इस के लिए वित्त प्राप्त करना। इस अंतर को कम करने के लिए आवश्यक कदमों में शामिल हैं - वृद्ध लोगों से जुड़े मुद्दों पर शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए और इस ज्ञान को अन्य केंद्रों तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षित लोगों के लिए आवश्यक धन जुटाना। टाटा मेमोरियल अस्पताल में, धनी रोगियों द्वारा गरीब रोगियों के लिए एक रोगी समर्थित निधि शुरू की गई है।
पुख्ता सबूतों का अभाव एक और समस्या है। क्लीनिकल ट्रायल कैंसर उपचार विकल्पों और साक्ष्य-आधारित दवाओं की आधारशिला हैं। ऐसे शोध में शामिल कैंसर रोगी युवा हैं और इसलिए ऐसे शोध से प्राप्त उपचार संबंधी ज्ञान कैंसर वाले बुजुर्गों के लिए साक्ष्य-आधारित नहीं माना जा सकता है। वृद्ध रोगियों पर अध्ययन करने के लिए धन की आवश्यकता है। जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए इस क्षेत्र के लिए वकालत करना और इस से संबंधित अध्ययन के लिए धन प्राप्त करना दो बड़ी ज़रूरतें हैं।
क्लिनिक आने वाला कैंसर वाले लोगों में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति वृद्ध होता है। इसलिए इन लोगों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी क्षेत्र को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है।
मुख्य संदे
- यदि आप बुजुर्ग हैं और आपको कैंसर हैं या आप ऐसे किसी व्यक्ति के देखभालकर्ता हैं, या किसी ऐसे बुजुर्ग को जानते हैं जिन्हें कैंसर है, तो कम से कम एक बार जेरीऐट्रिक मूल्यांकन के लिए किसी जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने का प्रयास करें।
- अपने अस्पताल को जराचिकित्सा क्लिनिक शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कैंसर वाले बुजुर्गों की देखभाल और उन से संबंधित अनुसंधान के लिए धन की आवश्यकता है।
डॉ. वनिता नोरोन्हा एक अग्रणी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और शोधकर्ता हैं, जिन्हें सिर और गर्दन, वक्ष, जननांग कैंसर, प्रीसिशन मेडिसन, और जेरीऐट्रिक ऑन्कोलॉजी के प्रबंधन में व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त है। वे टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। उनका शैक्षणिक कार्य क्लीनिकल ट्रायल ट्रांसलेशनल रिसर्च और सीमित संसाधन वाली परिस्थितियों के अनुरूप लागत-प्रभावी कैंसर उपचार प्रोटोकॉल के विकास तक फैला हुआ है।